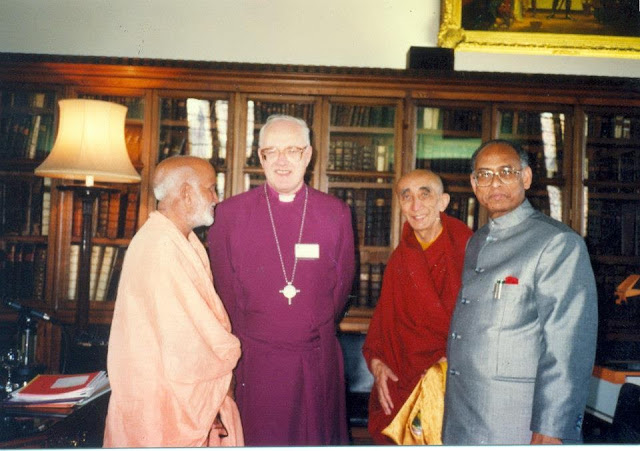राजविद्या-राजगुह्य योग और विनोबा भावे के विचार
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । ज्ञानं
विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ।।
राजविद्या
राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् । प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमाव्ययम् ।।1
श्रीमद्भगवद्गीता के नवम अध्याय में श्रीकृष्ण अर्जुन से
कहते हैं कि तुम दोषदृष्टि रहित हो, भक्त हो, इसलिए मैं इस परम गोपनीय ज्ञान को,
जो विज्ञानसम्मत और तर्कपूर्ण है, उसे बताऊँगा। तुम इस ज्ञान को जानकर इस दुःखरूपी
संसार से मुक्त हो जाओगे। यह विज्ञानसम्मत और तर्कपूर्ण ज्ञान सभी विद्याओं का
राजा है। यह समस्त गोपनीय ज्ञानों का राजा है। यह पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल
देने वाला, धर्म से युक्त है। यह सुगम और अविनाशी है। गीता का नवम अध्याय उस ज्ञान
की बात से शुरू होता है, जिसे विज्ञानसम्मत अर्थात तथ्यों पर खरा उतरने वाला बताया
गया है। यह अत्यंत गोपनीय भी है, अर्थात यह सर्वसुलभ नहीं है, किंतु इसे प्राप्त
करने का मार्ग जानकर और उस मार्ग पर चलकर यदि इस विज्ञानसम्मत ज्ञान को ग्रहण कर
लिया जाए, इसे जीवन में उतार लिया जाए, तो यह सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा, इसके
प्रत्यक्ष फल प्राप्त होंगे। धर्म से युक्त ऐसे विशिष्ट ज्ञान की विवेचना करने के
कारण गीता में इस अध्याय का अपना विशिष्ट स्थान है।
धर्म, आस्था और भक्ति के रूढ़ अर्थों से अलग गीता व्यवहार
की दृष्टि से, दैनंदिन जीवन के कार्य-व्यापार की दृष्टि से भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण
है। विभिन्न भाष्यकारों, विद्वानों और तर्कशास्त्रियों ने इस कारण गीता का समग्र
विवेचन विभिन्न तरीकों-पद्धतियों से किया है। विनोबा भावे द्वारा दिये गए गीता-प्रवचन
इस संदर्भ एकदम अलग स्थान रखते हैं। गीता के समस्त अध्यायों पर दिये गए उनके
प्रवचन पुस्तकाकार उपलब्ध हैं। अपने प्रवचनों को उन्होंने आम जनता के उपयोगार्थ
केंद्रित किया है। वे ‘गीता प्रवचन’ की प्रस्तावना में लिखते हैं- इनमें
तात्विक विचारों का आधार छोड़े बगैर, लेकिन किसी वाद में न पड़ते हुए, रोज के
कामों की बातों का ही जिक्र किया गया है।.... यहाँ श्लोकों के अक्षरार्थ की चिंता
नहीं, एक-एक अध्याय के सार का चितंन है। शास्त्र-दृष्टि कायम रखते हुए भी
शास्त्रीय परिभाषा का उपयोग कम-से-कम किया है। मुझे विश्वास है कि हमारे गाँव वाले
मजदूर भाई-बहन भी इसमें अपना श्रम-परिहार पाएँगे।2 इस प्रकार
विनोबा के गीता-प्रवचन की समाज से निकटता और उनके प्रवचनों की लौकिक दृष्टि स्वतः
प्रमाणित हो जाती है। पूज्य साने गुरुजी ने विनोबा के प्रवचनों को शब्दबद्ध किया।
मराठी और हिंदी में विनोबा का ‘गीता प्रवचन’ एक अलग किस्म के भाष्य के रूप में,
गीता को आत्मसात करने की नई दृष्टि के रूप में इस प्रकार सामने आ सका।
 बाबा विनोबा के लिए श्रीमद्भगवद्गीता जीवन का दर्शन-मात्र
नहीं है, वरन् जीवन को जीने की कला है, एक पद्धति है। वे इसी कारण गीता के विविध
अध्यायों का विवेचन शास्त्र के स्थान पर लोक के आधार पर करते हैं।
श्रीमद्भगवद्गीता का नवाँ अध्याय इस कारण उनके लिए विशिष्ट हो जाता है, क्योंकि वे
इस अध्याय के माध्यम से जीवन जीने की उस पद्धति को व्याख्यायित करते हैं, जो उनके
समय की अनिवार्यता और आवश्यकता थी। वे गीता के नवम अध्याय पर प्रवचन की शुरुआत में
ही कहते हैं-
बाबा विनोबा के लिए श्रीमद्भगवद्गीता जीवन का दर्शन-मात्र
नहीं है, वरन् जीवन को जीने की कला है, एक पद्धति है। वे इसी कारण गीता के विविध
अध्यायों का विवेचन शास्त्र के स्थान पर लोक के आधार पर करते हैं।
श्रीमद्भगवद्गीता का नवाँ अध्याय इस कारण उनके लिए विशिष्ट हो जाता है, क्योंकि वे
इस अध्याय के माध्यम से जीवन जीने की उस पद्धति को व्याख्यायित करते हैं, जो उनके
समय की अनिवार्यता और आवश्यकता थी। वे गीता के नवम अध्याय पर प्रवचन की शुरुआत में
ही कहते हैं-
यह अध्याय गीता के मध्य भाग में खड़ा है। सारी महाभारत के
मध्य गीता और गीता के मध्य यह नवाँ अध्याय। अनेक कारणों से इस अध्याय को पावनता
प्राप्त हो गई है। कहते हैं कि ज्ञानदेव ने जब अंतिम समाधि ली, तो उन्होंने इस
अध्याय का जप करते हुये प्राण छोड़ा था। इस अध्याय के स्मरण मात्र से मेरी आँखें
छलछलाने लगती हैं और दिल भर आता है। व्यासदेव का यह कितना बड़ा उपकार है, केवल
भारतवर्ष पर ही नहीं, सारी मनुष्य-जाति पर उनका यह उपकार है। जो अपूर्व बात भगवान
ने अर्जुन को बताई, वह शब्दों द्वारा प्रकट करने योग्य न थी। परंतु दयाभाव से
प्रेरित होकर व्यासजी ने इसे संस्कृत भाषा द्वारा प्रकट कर दिया। गुप्त वस्तु को
वाणी का रूप दिया। इस अध्याय के आरंभ में भगवान कहते हैं-
राजविद्या
राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।
यह जो राजविद्या है, यह जो अपूर्व वस्तु है, वह प्रत्यक्ष
अनुभव करने की है। भगवान उसे ‘प्रत्यक्षावगम’ कहते हैं। शब्दों में न समाने वाली,
परंतु प्रत्यक्ष अनुभव की कसौटी पर कसी हुई यह बात इस अध्याय में बतायी गई है।
इससे यह बहुत मधुर हो गया है। तुलसीदासजी ने कहा है-
को जाने को जैहे
जम-पुर, को सुर-पुर पर-धाम को ।
तुलसिहि बहुत भलो लागत, जग-जीवन रामगुलाम को ।।
मरने के बाद मिलने वाले स्वर्ग और उसकी कथाओं से यहाँ क्या
काम चलेगा? कौन कह सकता है कि स्वर्ग कौन जाता है और यमपुर कौन जाता है? यदि संसार
में चार दिन रहना है, तो राम का गुलाम बनकर रहने में ही मुझे आनंद है, ऐसा
तुलसीदासजी कहते हैं। राम का गुलाम होकर रहने की मिठास इस अध्याय में है।
प्रत्यक्ष इसी देह में, इन्हीं आँखों से अनुभूत होने वाला फल, जीते जी अनुभव की जाने
वाली बातें इस अध्याय में बतायी गयी हैं।3
नवम अध्याय में श्रीकृष्ण द्वारा कहे गए कथनों का ऐसा
विश्लेषण अद्भुत है। तुलसी के राम जहाँ मर्यादा और आदर्श के प्रतीक हैं, वहीं
विनोबा के राम मानव-मात्र हैं, जीव-मात्र हैं। यह जगत इसी कारण राममय है। मानव
साक्षात् परमात्मा की ही मूर्ति है, इसलिए उसकी सेवा, उसकी भक्ति ही सबसे बड़ी है।
संसार में जो प्रत्यक्ष है, उसकी सेवा पर हमें एकाग्र होना चाहिए। स्वर्ग, नर्क की
कल्पनाओं में उलझकर अपने सांसारिक कर्मों को जटिल, आत्मकेंद्रित और कृत्रिम नहीं
बनाना चाहिए। इसके लिए विनोबा बड़ी सहजता के साथ कृष्ण का उदाहरण प्रस्तुत करते
हैं। वे कहते हैं कि- मोक्ष पर केवल मनुष्य का ही अधिकार नहीं, बल्कि पशु-पक्षी
का भी है- यह बात श्रीकृष्ण ने साफ कर दी है।4 इंद्र के स्थान पर
गोवर्धन पर्वत की पूजा का विधान श्रीकृष्ण ने इसीलिए बताया था। गोवर्धन पर्वत, जो
सबके सामने है, प्रत्यक्ष है। जिस पर हमारा जीवन आश्रित है, उसके प्रति हमें
कृतज्ञ होना चाहिए। वह वास्तव में परमात्मा का रूप है। इसी तरह गाय-बैल-अश्व और
अन्य जीवधारी भी हैं। उनके प्रति समर्पण का भाव, उनके प्रति भक्ति का भाव रखना
सीधे परमात्मा की भक्ति है, क्योंकि वे परमात्मा के ही प्रतिरूप हैं।
कौन्तेय ! जो खाते हो करते तथा आहुति जो करो ।
दान तप जो करो
वह सब मुझे
ही अर्पण करो ।।
शुभ अशुभ जो फल कर्म बंधन यह किये से मुक्त हों ।
कर्म सब अर्पण करो,
मुझसे मिलो अरु मुक्त हो ।।5
श्रीमद्भगवद्गीता के नवम अध्याय में कर्मयोग और भक्तियोग का
सुंदर मेल है। कर्मयोग कर्म करने और फल की इच्छा न करने की बात कहता है। भक्तियोग
ईश्वर के साथ भावपूर्ण जुड़ाव की बात कहता है। दोनों ही अलग-अलग दिशाओं पर
केंद्रित हैं। नवम अध्याय में इन दोनों को इस प्रकार समीप लाया गया है, जोड़ दिया
गया है, कि यह राजयोग बन गया है। यह योग गुह्य भी इसी कारण है, क्योंकि प्रत्यक्ष
प्रदर्शित कर्मयोग और भक्तियोग का प्रत्यक्ष नहीं रह जाता, गोपनीय हो जाता है। यह
जटिल साधना के साथ अंतरात्मा में केंद्रित हो जाता है। यह भक्ति और कर्म के
सौंदर्य को आत्म-तत्त्व के सौंदर्य से जोड़कर श्रेष्ठतम बना देता है। बाबा विनोबा
ने दैनंदिन जीवन के कार्य-व्यवहार में इस श्रेष्ठता को प्रतिष्ठापित करने हेतु
राजयोग की अत्यंत सामयिक और सुंदर व्याख्या की है। वे लिखते हैं- फल का विनियोग
चित्त-शुद्धि के लिए करना चाहिये। जो काम जैसा हो जाय, वैसा ही उसे भगवान को अर्पण
कर दो। प्रत्यक्ष क्रिया जैसे-जैसे होती जाय, वैसे-ही-वैसे उसे भगवान को अर्पण
करके मनरतुष्टि प्राप्त करते रहना चाहिए। फल को छोड़ना नहीं है, उसे भगवान को
अर्पण कर देना है। यह तो क्या, मन में उत्पन्न होने वाली वासनाएँ और काम-क्रोधादि
विकार भी परमेश्वर को अर्पण करके छुट्टी पाना है।6 इस प्रकार के
भाव के साथ कर्म किया जाए, तो आज के समय की अनेक विकृतियों का शमन किया जा सकता
है। भगवान को अर्पित करने के लिए भक्त जिस प्रकार शुद्ध पुष्प, जल, प्रसाद आदि का
यत्न करते हैं, उसी प्रकार शुद्ध और सात्विक कर्मों के अर्पण हेतु वे प्रेरित
होंगे। कर्म में शुचिता और पवित्रता स्वतः आ जाएगी। शरीर की प्रत्येक इंद्रिय
द्वारा किया गया कार्य ईश्वर को अर्पण किया जाना है, यह मन में रखकर कार्य करना ही
‘राजयोग’ है। बाबा विनोबा द्वारा की गई ऐसी व्याख्या अद्भुत और अनुपम है। वे कहते
हैं कि अर्पण करने हेतु विशिष्ट क्रिया का आग्रह नहीं है। कर्ममात्र ईश्वर को
अर्पित कर देना है।
विनोबा ने सारे जीवन को हरिमय बनाने, अर्थात पावन-पुनीत
बनाने का माध्यम राजयोग को ही बताया है। जीवन के हर क्षेत्र में इसकी उपादेयता को,
इसकी प्रासंगिकता को वे सरल शब्दों में स्पष्ट करते हैं। वे घर-परिवार से लगाकर
समाज तक हर क्षेत्र में इसकी उपादेयता को व्याख्यायित करते हैं। अध्ययन-अध्यापन
में राजयोग की महत्ता को विशेष रूप से वे रेखांकित करते हैं। वे कहते हैं कि- शिक्षण-शास्त्र
में तो इस कल्पना की बड़ी ही आवश्यकता है, लड़के क्या हैं, प्रभु की मूर्तियाँ
हैं। गुरु की यह भावना होनी चाहिये कि मैं इन देवताओं की ही सेवा कर रहा हूँ। तब
वह लड़कों को ऐसे नहीं झिड़केगा- “चला जा अपने घर। खड़ा रह घंटे भर। हाथ लवाकर।
कैसे मैले कपड़े हैं? नाक से कितनी रेंट बह रही है।” बल्कि हलके हाथ से नाक साफ कर
देगा, मैले कपड़े धो देगा और फटे कपड़े सीं देगा। यदि शिक्षक ऐसा करे, तो इसका
कितना अच्छा परिणाम होगा। मार-पीटकर कहीं अच्छा नतीजा निकाला जा सकता है? लड़कों
को भी चाहिये कि वे इसी दिव्य भावना से गुरु को देखें। गुरु शिष्य को हरि मूर्ति
और शिष्य गुरु को हरि मूर्ति मानें। परस्पर ऐसी भावना रखकर यदि दोनों व्यवहार करें,
तो विद्या तेजस्वी होगी।7
विनोबा का मत है कि ऐसी भावना के साथ जब जीवन में कर्म किये
जाएँगे, तब कर्म स्वयं पवित्र हो जाएगा और पाप का भय नहीं रह जाएगा। सब जगह
प्रभु विराजमान हैं, ऐसी भावना चित्त में बैठ जाय, तो फिर एक-दूसरे के साथ हम कैसा
व्यवहार करें, यह नीतिशास्त्र हमारे अंतःकरण में अपने आप स्फुरने लगेगा।8
ऐसी भावना को कर्म में उतारने के बाद नीतिशास्त्र और व्यवहार-विज्ञान के विशिष्ट
अध्ययन की अनिवार्यता नहीं रह जाती है। जब कर्म पवित्र हो जाएगा, तब पाप और पुण्य
का अंतर करने की आवश्यकता भी नहीं रह जाएगी। कर्म स्वतः पुण्यमय और पवित्र हो
जाएगा।
इसी आधार पर वे जीवन की सार्थकता को प्रमाणित करते हैं। वे
लिखते हैं- गीता में कुल सात सौ ही श्लोक हैं। पर ऐसे भी ग्रंथ हैं, जिनमें
दस-दस हजार श्लोक हैं। किंतु वस्तु का
आकार बड़ा होने से उसका उपयोग भी अधिक होगा, ऐसा नहीं कह सकते। देखने की बात यह है
कि वस्तु में तेज कितना है, सामर्थ्य कितनी है? जीवन में क्रिया कितनी है, इसका
महत्त्व नहीं। ईश्वरार्पण-बुद्धि से यदि एक भी क्रिया की हो, तो वही हमें पूरा
अनुभव करा देगी।9 इस प्रकार जीवन में विशिष्ट की प्राप्ति के लिए,
मोक्ष के लिए अलग से यत्न करने की, प्रयास करने की बात बाबा विनोबा नहीं करते। वे
जीवन के किसी भी क्षेत्र में, कर्म के किसी भी स्तर पर, किसी भी क्षण पवित्र भावना
से कर्म करने और उसे ईश्वर को अर्पित कर देने की क्रिया को ही श्रेष्ठ बताते हैं।
वे कहते हैं कि- बोने और फेंक देने में फर्क है। बोया हुआ थोड़ा भी अनंतगुना
होकर मिलता है। फेंका हुआ यों ही नष्ट हो जाता है। जो कर्म ईश्वर को अर्पण किया
गया है, उसे बोया हुआ समझो। उससे जीवन में अनंत आनंद भर जायगा, अपार पवित्रता छा
जायगी।10
 भक्तियोग और कर्मयोग के संयोजन से निःसृत राजयोग की सुंदर,
सहज और व्यावहारिक व्याख्या करके बाबा विनोबा ने श्रीमद्भगवद्गीता के उस लोकोपयोगी
पक्ष को प्रकाश में लाने का कार्य किया है, जिसे जीवन जीते हुए, सरल और सहज साधना
के साथ आत्मसात् किया जा सकता है। आज के जीवन में इसकी प्रासंगिकता समाज के
निर्माण के लिए, जीवन की शुचिता के लिए, व्यवहार की पवित्रता के लिए, समर्पण और
त्याग के साथ संबंधों के निर्वहन के लिए, और सच्चे अर्थों में मोक्ष की प्राप्ति
के लिए है।
भक्तियोग और कर्मयोग के संयोजन से निःसृत राजयोग की सुंदर,
सहज और व्यावहारिक व्याख्या करके बाबा विनोबा ने श्रीमद्भगवद्गीता के उस लोकोपयोगी
पक्ष को प्रकाश में लाने का कार्य किया है, जिसे जीवन जीते हुए, सरल और सहज साधना
के साथ आत्मसात् किया जा सकता है। आज के जीवन में इसकी प्रासंगिकता समाज के
निर्माण के लिए, जीवन की शुचिता के लिए, व्यवहार की पवित्रता के लिए, समर्पण और
त्याग के साथ संबंधों के निर्वहन के लिए, और सच्चे अर्थों में मोक्ष की प्राप्ति
के लिए है।
संदर्भ-
1. श्रीमद्भगवद्गीता, गीताप्रेस, गोरखपुर, पृ. 117,
2. गीता प्रवचन, विनोबा, अनुवादक- हरिभाऊ उपाध्याय, अखिल भारत
सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, काशी, सं. 1956, प्रस्तावना,
3. गीता प्रवचन, विनोबा, अनुवादक- हरिभाऊ उपाध्याय, अखिल भारत
सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, काशी, सं. 1956, पृ. 122-123,
4. वही, पृ. 126,
5. श्रीमद्भगवद्गीता का पद्यानुवाद, गणेश मिश्र ‘बनरा’, साहित्य
मंदिर प्रेस, लखनऊ, प्रथम सं. 1937, पृ. 33-34,
6. गीता प्रवचन, विनोबा, अनुवादक- हरिभाऊ उपाध्याय, अखिल भारत
सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, काशी, सं. 1956, पृ. 130,
7. वही, पृ. 138
8. वही, पृ. 139,
9. वही, पृ. 141,
10. वही,
पृ. 141 ।
डॉ. राहुल मिश्र
(अखिल
भारतीय साहित्य परिषद् व गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के संयुक्त तत्त्वावधान में
नई दिल्ली में दिनांक 25-26 मार्च, 2018 को आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में
प्रस्तुत शोध-पत्र)